Ras किसे कहते हैं | रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण: नमस्कार दोस्तों ! हिंदी व्याकरण के एक और नोट में आप सभी का स्वागत है। Poems Wala के इस ब्लॉग में हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानने वाले हैं। इसमें Ras ka arth, Ras ki paribhasha, Ras ke bhed, Ras ke ang, और Ras ke prakar के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काव्य में रस का एक अहम योगदान होता है। इसकी भूमिका इस बात से समझी जा सकती है कि इसे काव्य की आत्मा कहा जाता है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं..
रस का अर्थ क्या होता है | Ras ka arth kya hota hai
हिंदी भाषा में रस का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से रचनाकार अपने दर्शकों की भावनाओं को स्पष्ट करते हैं और उन्हें आनंद, सुंदरता और उत्कटता का अनुभव कराते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है – ‘आनन्द’। रस एक अद्भुत और प्रभावशाली अनुभव है जिसे कविता, गीत, नाटक और कहानी आदि में व्यक्त किया जाता है। यह रस संग्रह के रूप में माना जाता है, जिसमें भावों और आनंद की विविधता होती है।
रस क्या करते हैं? | Ras kya karte hain
रस साहित्यिक रचनाओं को गहराई प्रदान करते हैं और उसे अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो रस एक ऐसा तत्व है जो साहित्यिक कार्यों को जीवंत और सांस्कृतिक बनाता है। यह भाषा के साथ रंग, भाव, आनंद और रोमांच का आदान-प्रदान करता है। इसलिए, हिंदी भाषा में रस एक महत्वपूर्ण अंश है जो साहित्य को संजीवनी देता है और उसे जनसाधारण तक पहुंचाता है।
रस की परिभाषा | Ras ki Paribhasha
Ras kise kahte hain- “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः।” अर्थात् विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनन्द ही Ras kahte hain.
Ras ki paribhasha- भरतमुनि ने अपने ‘नाट्यशास्त्र’ में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है – साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटकादि को देखने से जो आनन्द की अनुभूति होती है, उसे ‘रस’ कहते हैं।

रस के अंग | Ras ke Ang
रस के मुख्य रुप से चार अंग या तत्व माने जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं –
1. स्थायी भाव – मानव ह्रदय मे स्थायी रूप मे विद्यमान रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते है। यीभाव रस को विद्रुमा भी कहा जाता है। यह रस वह होता है जो पाठक के मन में स्थिर भाव उत्पन्न करता है और उसे उस स्थिति में लगातार रहने का आनंद प्रदान करता है। स्थायीभाव रस प्रेम, उत्साह, शान्ति, अभिमान, श्रद्धा और भक्ति जैसे भावों को व्यक्त कर सकता है।
स्थायी भावों की संख्या नौ है –
| संख्या | रस | स्थायी भाव |
| 1 | श्रृंगार रस | रति |
| 2 | हास्य | हास |
| 3 | करूण | शोक |
| 4 | रौद्र | क्रोध |
| 5 | वीर | उत्साह |
| 6 | भयानक | भय |
| 7 | वीभत्स | जुगुप्सा (घृणा) |
| 8 | अद्भूत | विस्मय |
| 9 | शांत | निर्वेद (वैराग) |
2. विभाव – जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव रस हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण रस है। यह रस वह होता है जो पाठक के मन में विभावना या भावुकता की अनुभूति प्रकट करता है। विभाव रस के माध्यम से कवि या लेखक पाठक की भावनाओं को गहराई से समझते हैं और प्रकट करते हैं।
विभाव दो प्रकार के होते हैं
(i) आलम्बन विभाव- जिन वस्तुओं या विषयों पर आलम्बित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं; जैसे – नायक – नायिका।
आलम्बन के दो भेद हैं –
क. आश्रय – जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं।
ख. आलम्बन (विषय) – जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आलम्बन या विषय कहते हैं।
(ii) उद्दीपन विभाव- स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारक उद्दीपक विभाव कहलाते है।
3. अनुभाव – यह रस वह होता है जो पाठक के मन में सहजता और सहजता की अनुभूति को जगाता है। अनुभाव रस के माध्यम से पाठक पठन में स्थानिकता और आत्मीयता का अनुभव करता है। आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में शीरीरकि व मानसित चेष्टाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं।
अनुभाव चार प्रकार के माने गए है – कायिक (शारीरिक चेष्टाये जैसे – इशारे, उच्छवास, कटाक्ष), मानसिक, आहार्य और सात्विका सात्विक अनुभाव की संख्या आठ है, जो निम्न प्रकार है –
- स्तम्भ
- स्वेद
- रोमांच
- स्वर – भंग
- कम्प
- विवर्णता (रंगहीनता)
- अक्षु
- प्रलय (संज्ञाहीनता)
4. संचारी भाव (व्यभिचारी भाव) – संचारी भाव उस रस को कहते हैं जो पाठक के मन में विचारों, अनुभवों और भावनाओं की संचार या प्रसारण का कार्य करता है। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। इस रस के माध्यम से लेखक पाठक के मन में भावों को व्यक्त करता है और उन्हें प्रभावित करता है।
संचारी भावों की संख्या 33 है – हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा (व्रीड़ा), ग्लानि, चिन्ता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहित्था, अपस्मार, व्याधि, मरण।
आचार्य देव कवि ने ‘छल’ को चौतीसवाँ संचारी भाव माना है।
रस के प्रकार | Ras ke prakar
रस के प्रमुख प्रकार शृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीभत्स और आद्भुत होते हैं। रस वाचकों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है, जो उन्हें आनंदित और प्रभावित करता है।
1. शृंगार रस
जब प्रेमियों में सहज रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आस्वाद के योग्य (आनंद प्राप्त करने योग्य) हो जाता है, तो उसे शृंगार रस कहते हैं।
श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि प्रदान की गयी है। इस रस मे नायक-नायिका के संयोग (मिलन) की स्थिति का वर्णन होता हैं। शृंगार रस में सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं।
इसके प्रमुखत: दो भेद बताये गये हैं:-
(i) संयोग श्रृंगार (संभोग श्रृंगार) – जब नायक-नायिका के मिलन की स्थिति की व्याख्या होती है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है।
एक पल मेरे प्रिया के दूग पलक,
थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे।
चपलता ने इस विकंपित पुलक से,
दृढ़ किया मानो प्रणय सम्बन्ध था ॥ – सुमित्रानन्दन पन्त
(ii) वियोग श्रृंगार (विप्रलम्भ श्रृंगार) – जहाँ नायक-नायिका के विरह-वियोग, वेदना की मनोदशा की व्याख्या हो, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है।
अँखियाँ हरि दरसन की भूखीं।
कैसे रहें रूप-रस राँची ये बतियाँ सुन रूखीं।
अवधि गनत इकटक मग जोवत, तन ऐसी नहि भूखीं।
-सूरदास
2. करुण रस
वैभव का नाश, अनिष्ट की प्राप्ति, प्रेम पात्र का वियोग, प्रियजन की पीड़ा अथवा मृत्यु की प्राप्ति आदि से जहाँ शोक भाव की परिपूष्टि होती है, वहाँ करुण रस होता है। करुण रस जीवन में सहानुभूति की भावना का विस्तार करता है तथा मनुष्य को भोग की अपेक्षा साधना की ओर अग्रसर करता है।उदाहरण –
धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ
मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ
सीता गई तुम भी चले मै भी न जिऊंगा यहाँ
सुग्रीव बोले साथ में सब (जायेंगे) जाएँगे वानर वहाँ
3. हास्य रस
हास्य रस मनोरंजक है। यह नव रसों के अंतर्गत स्वभावत: सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है। इसका स्थायी भाव हास है। जब नायक – नायिका में कुछ अनौचित्य का आभास मिलता है, तो यह भाव जागृत हो जाता है। साधारण से भिन्न व्यक्ति, वस्तु, आकृति, विचित्र वेशभूषा, असंगत क्रियाओं, विचारों, व्यापारों, व्यवहारों को देखकर जिस विनोद भाव का संचार होता है, उसे हास कहते हैं।
हास्य दो प्रकार का होता है:- आत्मस्थ और परस्त
आत्मस्थ हास्य केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से उत्पन्न होता है, जबकि परस्त हास्य दूसरों को हंसते हुए देखने से प्रकट होता है। उदाहरण:-
बन्दर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने चले गंगा ।
बच्चो को छोड़ेंगे घर पे वही करेंगे हुडदंगा ।।
4. वीर रस
युद्ध अथवा शौर्य पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है, उस रस को उत्साह रस कहते है। उत्साह के चार क्षेत्र पाए गए हैं – युद्ध, धर्म, दया और दान। जब इन क्षेत्रों में उत्साह रस की कोटि तक पहुँचता है, तब उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण –
बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी ।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झाँसी वाली रानी थी ।।
5. रौद्र रस
रस क्रोध के कारण उत्पन्न इन्द्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। किसी विरोधी, अपकारी, धृष्ट आदि के कार्य या चेष्टाएँ, असाधारण अपराध, अपमान या अहंकार, पूज्य जन की निंदा या अवहेलना आदि से उसके प्रतिशोध में जिस क्रोध का संचार होता है, वही रौद्र रस के रूप में व्यक्त होता है। उदाहरण –
सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे |
संसार देखे अब हमारे शत्रुरण में मृत पड़े ||
6. भयानक रस
डरावने दृश्य देखकर मन में भय उत्पन्न होता है। जब भय नामक स्थायीभाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब भयानक रस उत्पन्न होता है। उदाहरण –
एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय |
विकल बटोही बीच ही पर्यो मूरछा खाए ||
7. वीभत्स रस
वीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अत्यंत गंदे और घृणित दृश्य वीभत्स रस की उत्पत्ति करते हैं। गंदी और घृणित वस्तुओं के वर्णन से जब घृणा भाव पुष्ट होता है तब यह रस उत्पन्न होता है।
उदाहरण – महाभारत युद्ध के विवरण में भीम दु:शासन, को युद्ध में परास्त करते हैं, और उसका पेट फाड़कर, अंतड़ियाँ बाहर निकाल लेते हैं। यह वीभत्स रस का उदाहरण है।
सिर पर बैठो काग आंखें दोउ खात निकारत |
खींचत जीभहिं स्यार अतिहि आनन्द उर धारत ||
8. अद्भुत रस
इसका स्थायी भाव विस्मय है। किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर जो आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वही अद्भुत रस में परिणत होता है। उदाहरण –
देख यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया |
क्षणभर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया ||
9. शांत रस
जब मनुष्य मोह-माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है तो मनुष्य के मन को जो शान्ति मिलती है, उसे शांत रस कहते हैं।
उदाहरण –
सुत बनितादि जानि स्वारथ रत न करु नेह सबही ते।
अंतहिं तोहि तजेंगे पामर! तूं न तजै अबही ते।।
अब नाथहिं अनुराग जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते।
बुझे न काम, अगिनी ‘तुलसी’ कहुँ विषय भोग बहु घी ते।। – तुलसी (विनयपत्रिका)
10. वात्सल्य रस
माता पिता का अपने सन्तान के प्रति प्रेम, गुरु का अपने शिष्य के प्रति, बड़े भाई बहनों का अपने छोटे भाई बहनों के प्रति जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो नुज, शिष्य और सन्तान के प्रति प्रेम का भाव जहाँ पर पाया जाता है वहां पर वात्सल्य रस होता है।
उदाहरण –
दादा ने चंदा दिखलाया
नेत्र नीरयुत दमक उठे
धुली हुई मुसकान देखकर
सबके चेहरे चमक उठे।
11. भक्ति रस
जब काव्य में ईश्वर की भक्ति एवं महिमा का वर्णन किया जाए तो वहा पर भक्ति रस होता है। जब काव्य में ईश्वरीय कृपा, चमत्कार भक्तों की भक्ति का वर्णन सुनने के बाद ह्रदय में जो भाव उत्पन्न होता है, वह भक्ति रस कहलाता है।
उदाहरण –
यह घर है प्रेम का खाला का घर नाहीं
सीस उतारी भुई धरो फिर पैठो घर माहि।
यह घर है प्रेम का खाला का घर नाहीं
सीस उतारी भुई धरो फिर पैठो घर माहि।
उम्मीद है कि आपको ‘Ras किसे कहते हैं | रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण’ कविता पसंद आई होगी। चाहें तो आप हमें कमेंट कर फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप भी अपनी कविता या रचना हमारी साइट पर पोस्ट कराना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहां क्लिक करके लिंक पर जाकर गूगल फॉम को भरें और इंतजार करें। आप हमारी दूसरी साइट Ratingswala.com को भी विजिट कर सकते है। वहां, मूवी, टेक खबरों के साथ साथ उसकी रिविव पढ़ने को मिलेंगे।
ये भी पढ़ें: Muktak Kavya | मुक्तक काव्य; परिभाषा, प्रकार एवं उदाहरण
ये भी पढ़ें: Prabandh Kavya | प्रबंध काव्य ; परिभाषा, भेद व उदाहरण
ये भी पढ़ें: Alankar | अलंकार की परिभाषा, भेद व उदाहरण
FAQs-Ras
Ras किसे कहते हैं?
रस एक ऐसा तत्व है जो साहित्यिक कार्यों को जीवंत और सांस्कृतिक बनाता है। यह भाषा के साथ रंग, भाव, आनंद और रोमांच का आदान-प्रदान करता है।
रस की परिभाषा क्या है?
साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटकादि को देखने से जो आनन्द की अनुभूति होती है, उसे ‘रस’ कहते हैं।
रस कितने प्रकार के होते हैं?
रस के नौ प्रमुख प्रकार होते हैं: श्रृंगार, हास्य, वीर, भयानक, बीभत्स, रौद्र, वात्सल्य, अद्भुत, शांत, भक्ति और करुण।
रस के कितने अंग होते हैं?
रस के चार अंग होते हैं, जो इस प्रकार हैं: स्थायीभाव रस, अनुभाव रस, विभाव रस, संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव रस
रस का महत्व क्या है?
यह पाठकों को आनंदित करने, उन्हें भावनाओं के साथ जोड़ने और कवि/लेखक की भावनाओं को संचारित करने में मदद करता है।

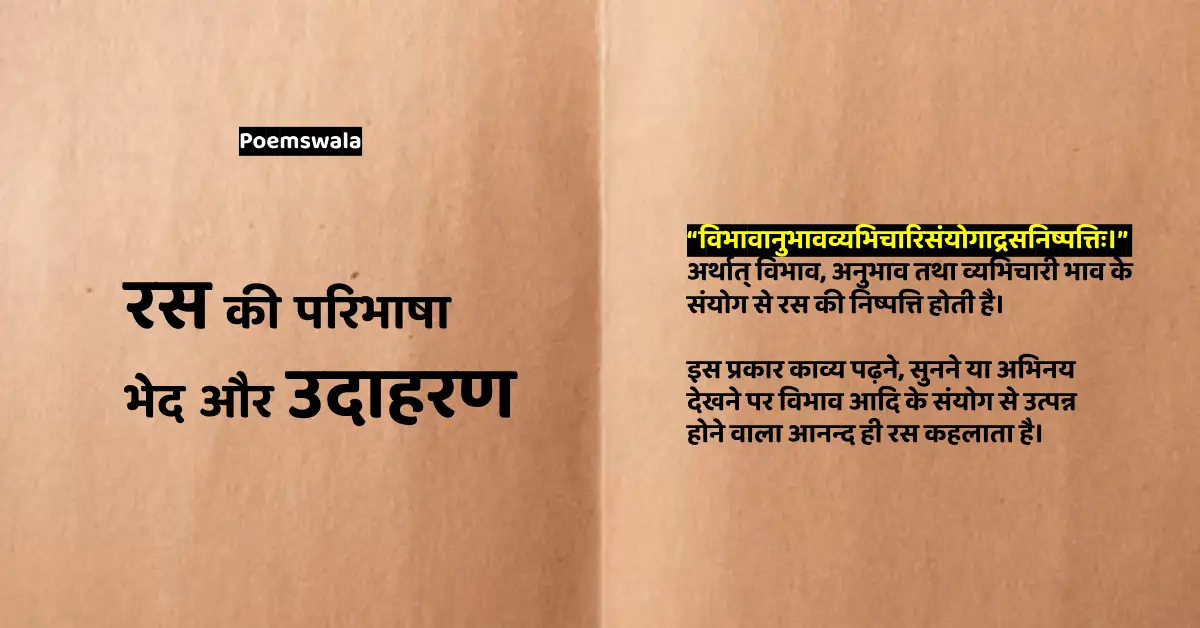

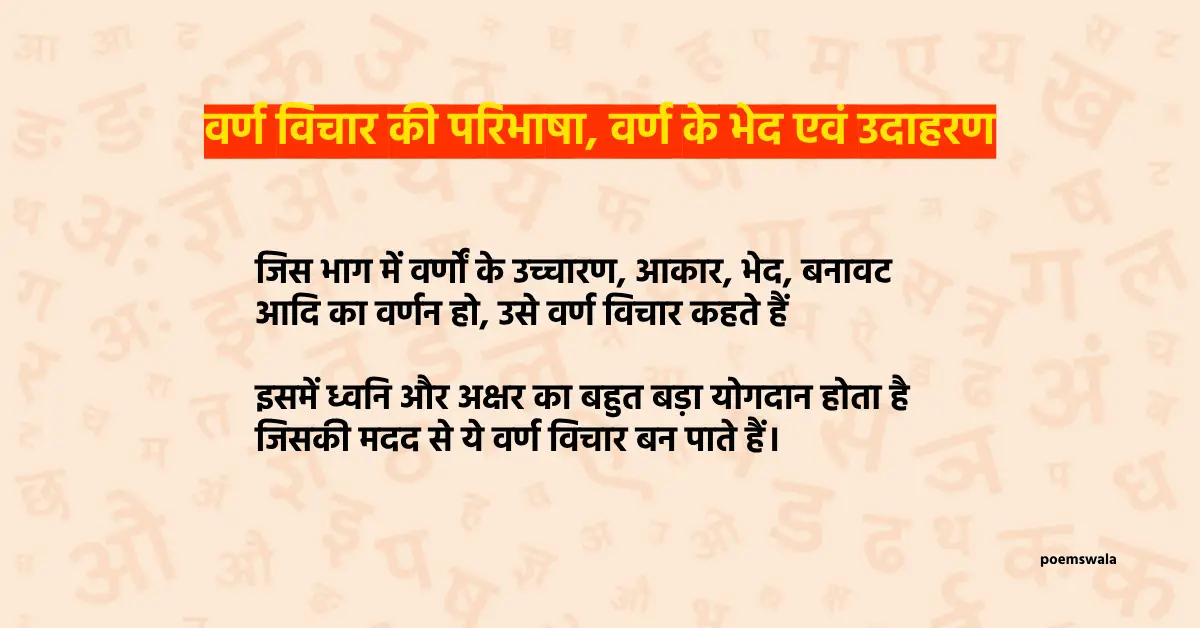
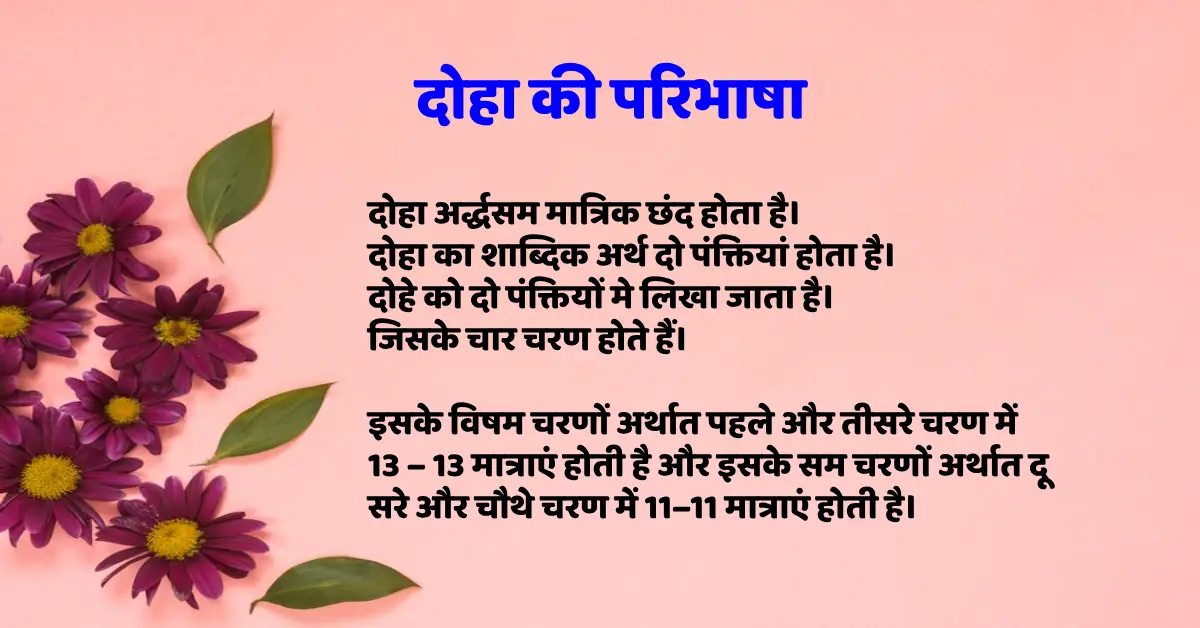
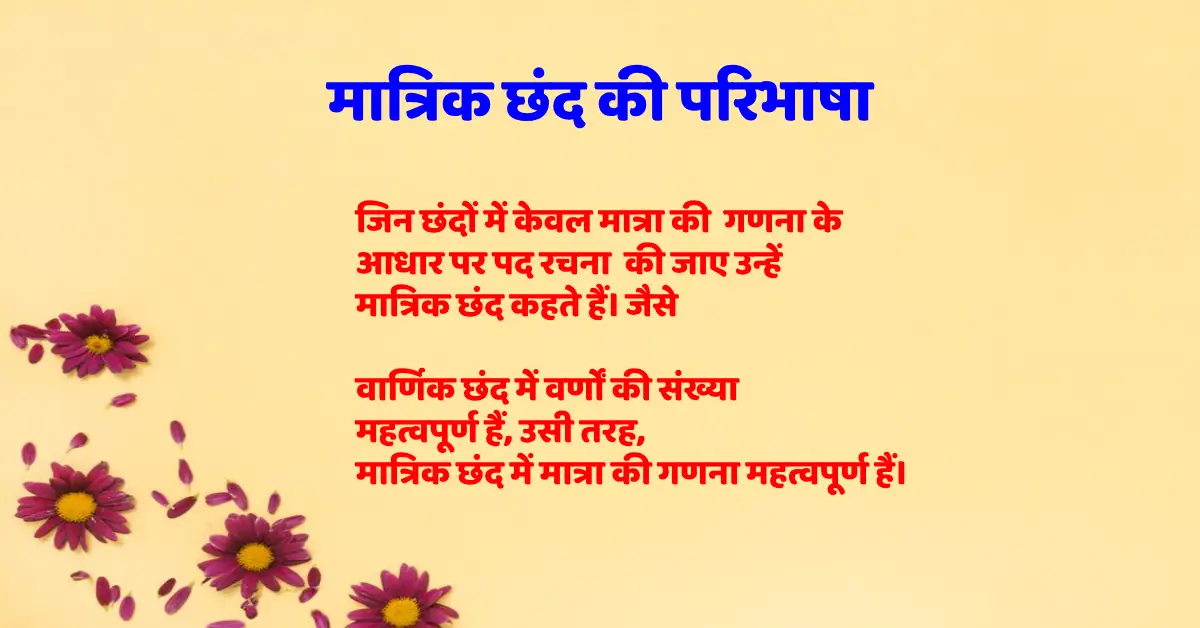



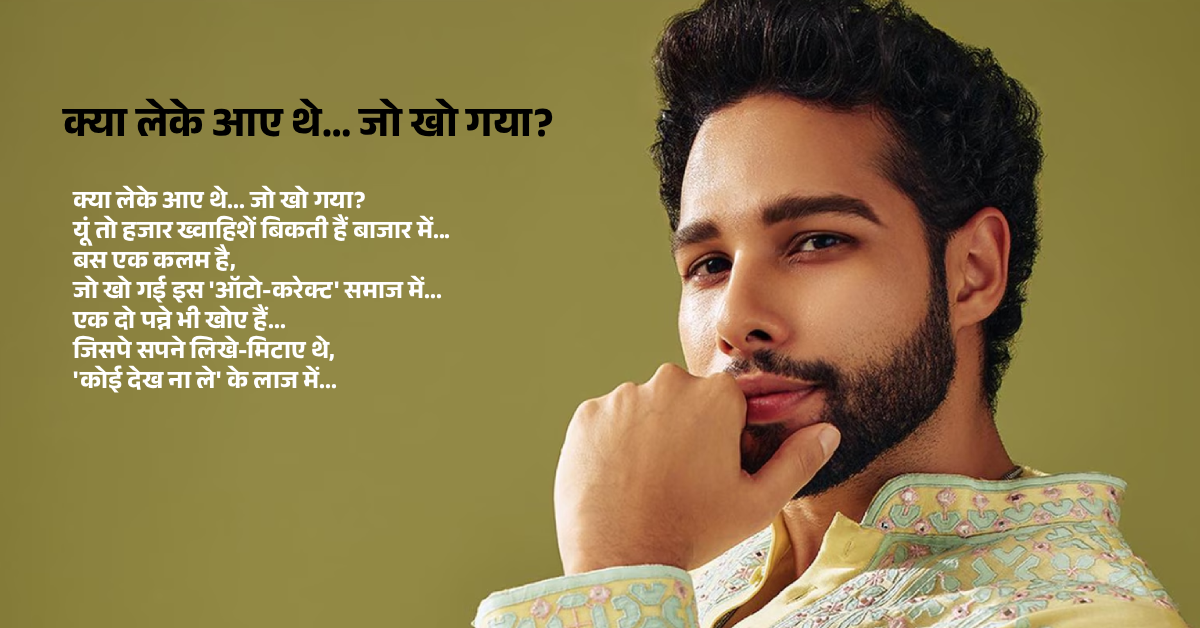
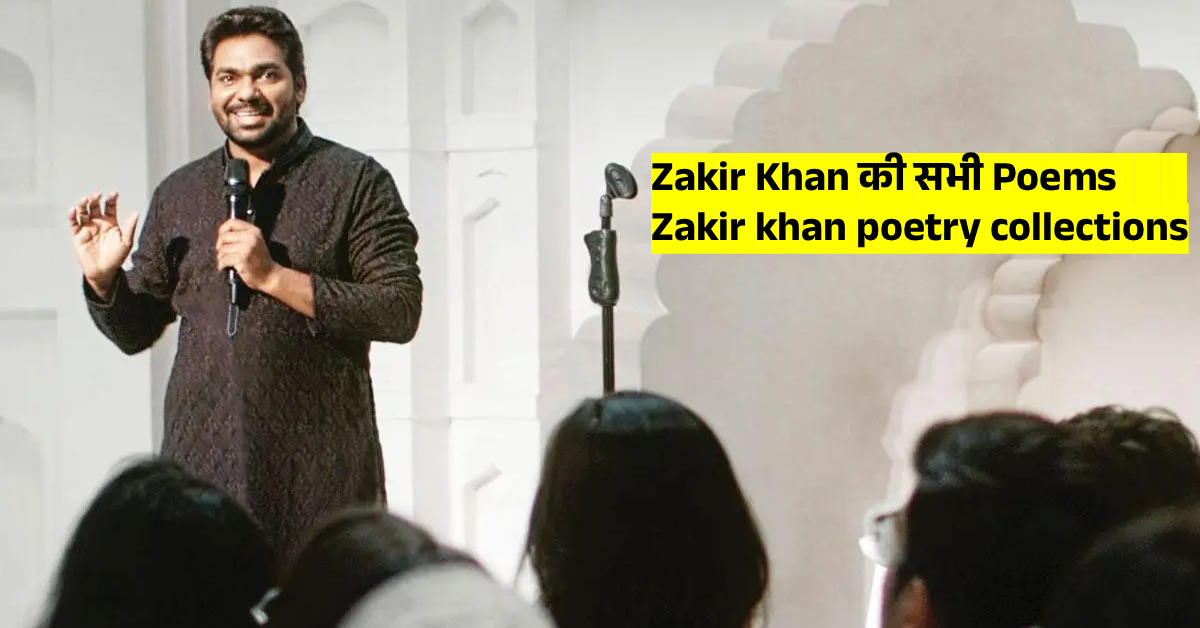
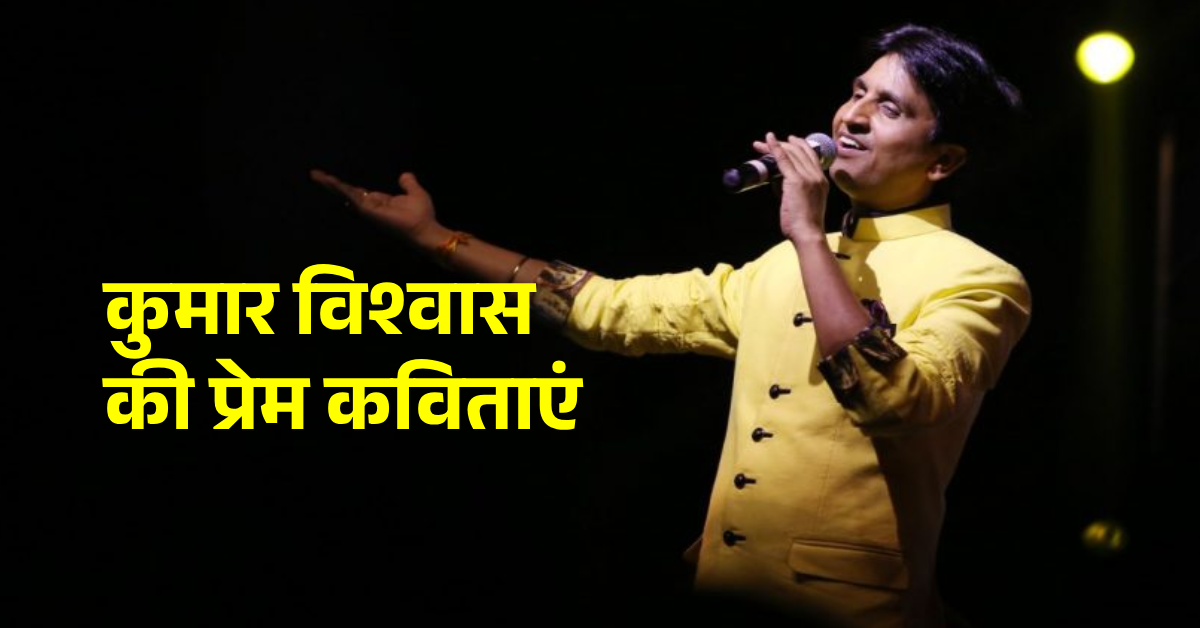
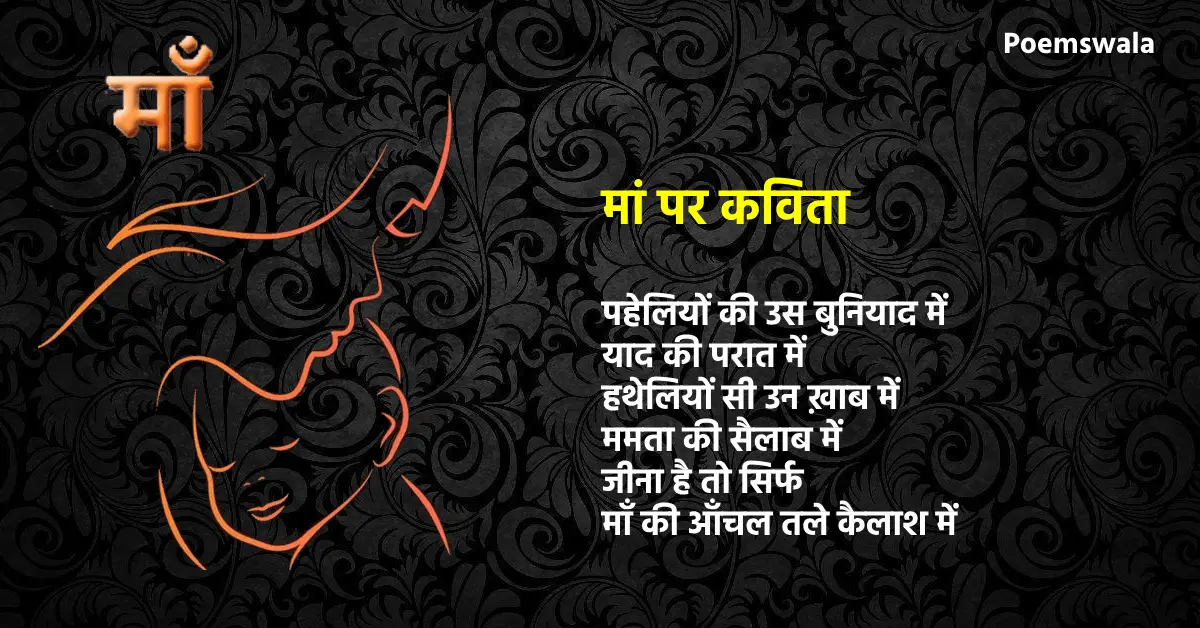
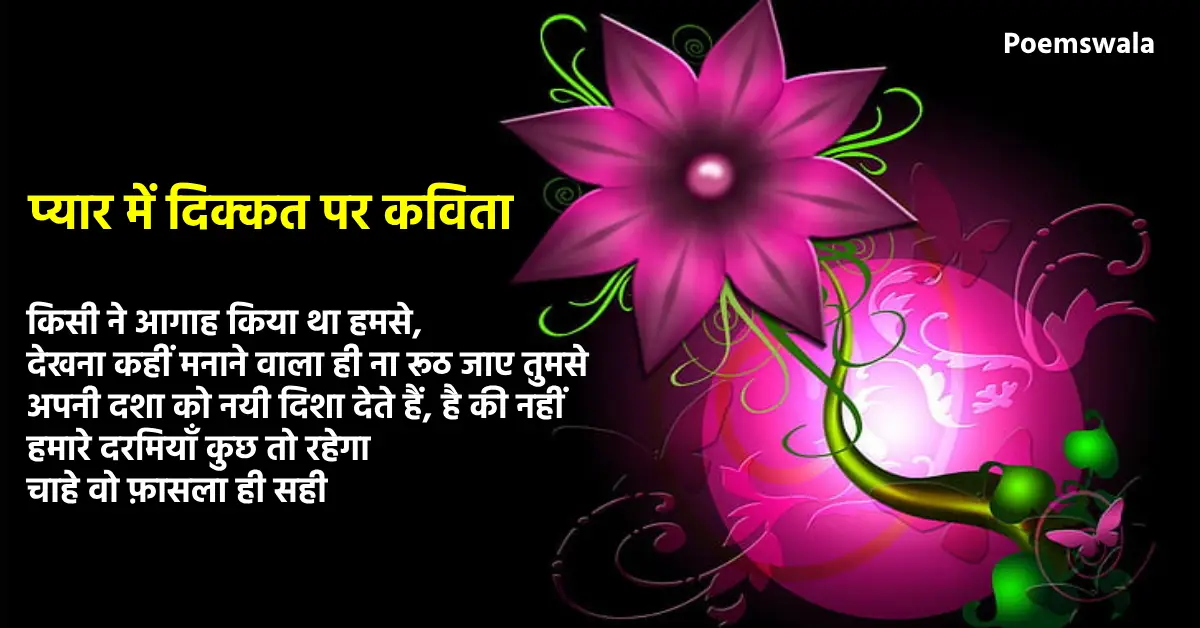
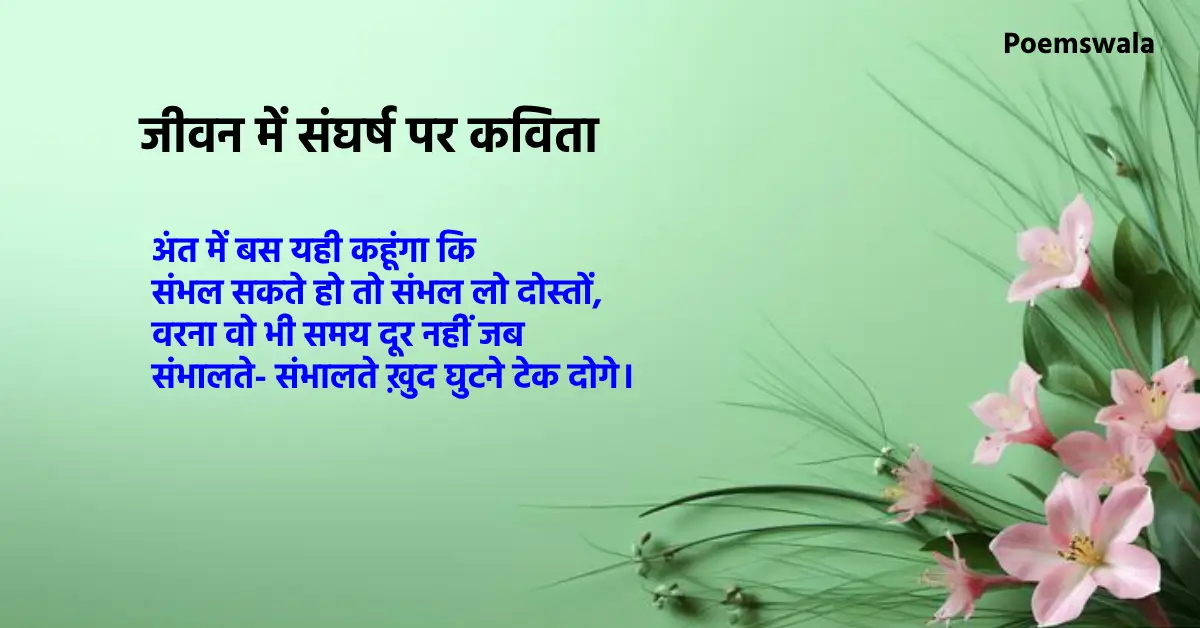
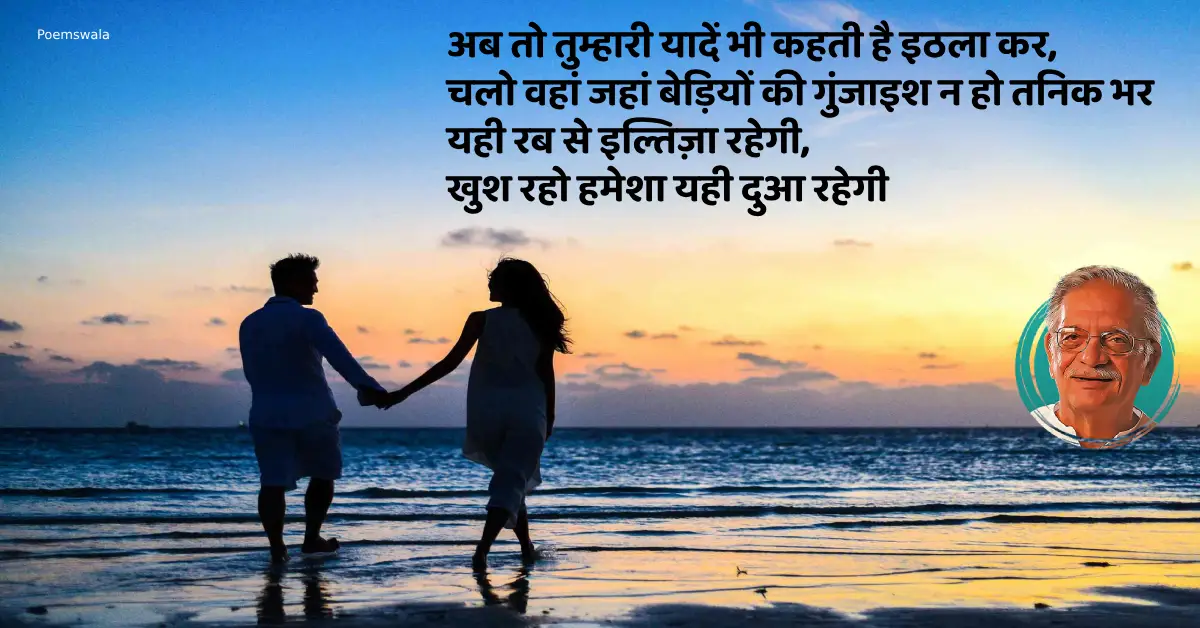
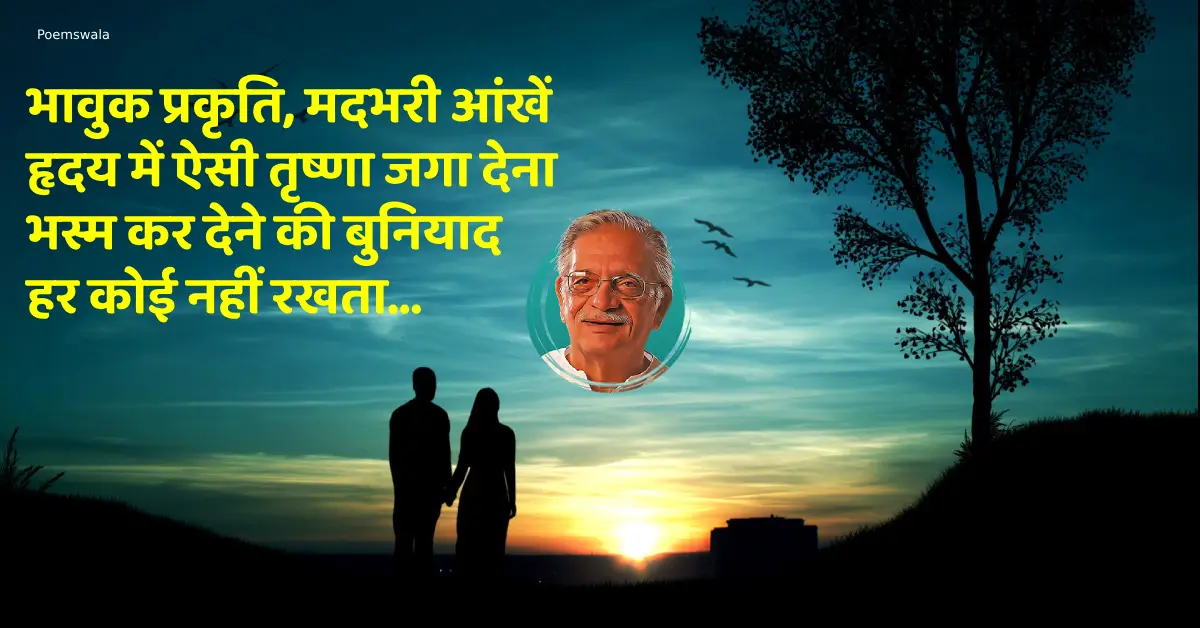
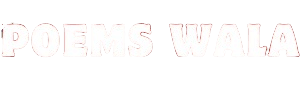
1 thought on “Ras किसे कहते हैं | रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण”